श्राद्ध का अध्यात्मशास्त्रीय महत्व
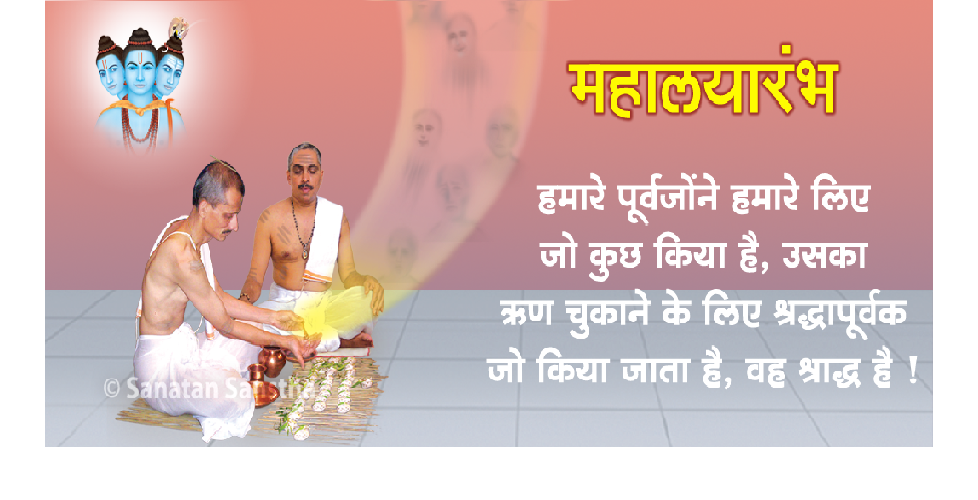
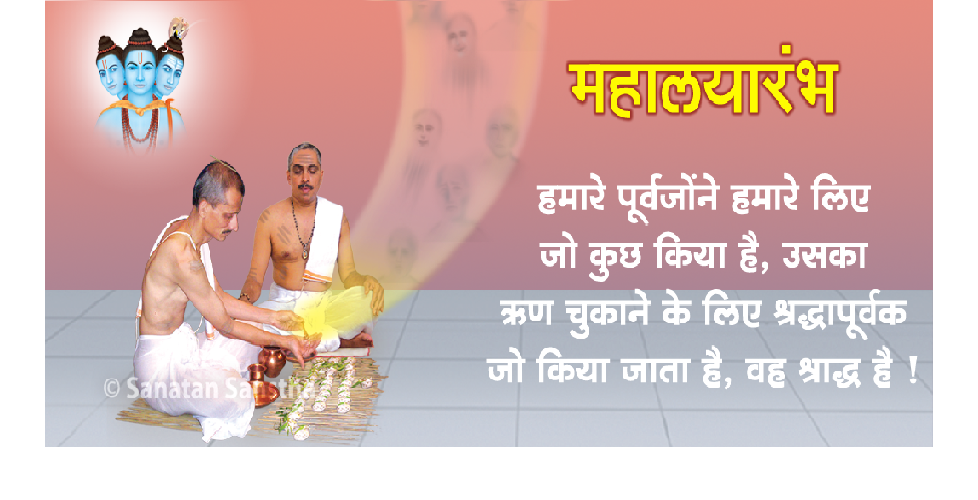
हिंदू धर्म में ईश्वर प्राप्ति के मूलभूत सिद्धांतों में से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है चार ऋण चुकाना। ईश्वर प्राप्ति हेतु प्रयास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को देवऋण, पितृऋण, ऋषिऋण और समाजऋण यह चार ऋण चुकाने पड़ते हैं। इसमें से पितरों का ऋण चुकाने के लिए पितरों के लिए श्राद्ध विधि करना आवश्यक होता है । माता-पिता और उसी प्रकार समीप के व्यक्तियों का मृत्यु पश्चात का प्रवास सुखमय और क्लेश रहित हो उन्हें सद्गति मिले इसलिए यह संस्कार अर्थात् श्राद्ध किया जाता है । इस वर्ष 10 सितंबर से 25 सितंबर तक का समय पितृ पक्ष है । हर वर्ष पितृ पक्ष की कृष्ण पक्ष में महालय श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध विधि यह हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण आचार है और वेद काल का आधार भी है । अवतारों ने भी श्राद्ध विधि किया था, यह उल्लेख पाया गया है ।
श्राद्ध के मंत्रो में पितरों को गति देने की सूक्ष्म शक्ति समाई रहती है । श्राद्ध का इतना महत्व होने पर भी आज हिंदुओं में धर्म शिक्षण का अभाव, उनका अध्यात्म के ऊपर अविश्वास आदि कारणों के कारण श्राद्ध विधि को नजरअंदाज व अनावश्यक कर्मकांड में गिना जाने लगा है । इसी कारण अन्य संस्कारो के जैसा श्राद्ध संस्कार भी अति आवश्यक किस प्रकार है यह बताना आवश्यक है । श्राद्ध का क्या अर्थ क्या है उसके पीछे का इतिहास, पितृपक्ष में श्राद्ध और दत्त का नामजप करने का महत्व, श्राद्ध विधि करने के पीछे का उद्देश्य, श्राद्ध किसने करना चाहिए ? श्राद्ध करने में अड़चन हो तो उसे दूर करने का तरीका आदि विषयों में जानकारी देने के लिए यह लेख संकलित किया गया है।
श्राद्ध शब्द की व्युत्पत्ति और अर्थ : ‘श्रद्धा’ इस शब्द से श्राद्ध शब्द का निर्माण हुआ है । भूलोक छोड़ कर गए हमारे माता-पिता ने हमारे लिए जो कुछ किया है उसका ऋण चुकाना असंभव है उनके लिए जो पूर्ण श्रद्धा के साथ किया जाता है वह श्राद्ध है ।
श्राद्ध शब्द की व्याख्या : ब्रह्म पुराण में श्राद्ध की व्याख्या इस प्रकार की गई है। देश, काल और योग्य स्थान को ध्यान में रखकर श्रद्धा और विधि से युक्त, पितरों के स्मरणार्थ ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता है उसको श्राद्ध कहते हैं ।
श्राद्ध विधि का इतिहास : श्राद्ध विधि की मूल कल्पना ब्रह्म देवता के पुत्र अत्रि ऋषि की है । अत्रि ऋषि ने अपने निमी नामक वंशज को ब्रह्मदेव द्वारा बताई गई श्राद्ध विधि सुनाई । वह परम्परा आज भी चालू है । मनु ने प्रथम बार श्राद्ध क्रिया की । इसलिए मनु को श्राद्धदेव कहते हैं । लक्ष्मण और जानकी जी के साथ राम जब वनवास के लिए गए तब भरत वनवास में उनसे भेंट करते हैं और उनको पिता के निधन का समाचार देते हैं उसके पश्चात राम जी उसी जगह पिता का श्राद्ध करते हैं, ऐसा उल्लेख रामायण में है । ऋग्वेद के समय समिधा और पिंड इसकी अग्नि में आहुति देकर की हुई पितरों की पूजा अर्थात अग्नौकरण, पिंड की तिल के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से की हुई पूजा अर्थात पिंड दान और ब्राह्मण भोजन इस क्रम से बनी श्राद्ध की तीन अवस्थाएं हैं । पूर्व समय की इन तीनों ही अवस्था को एकत्रित किया गया है । धर्म शास्त्र में यह श्राद्ध गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों को उनका कर्तव्य बताया गया है ।
।)
इस प्रकार इन सभी प्रकारों में से हर वर्ष श्राद्ध के दिन पितरों को स्मरण करके किसी भी प्रकार से श्राद्ध करना चाहिए । श्राद्ध किए बिना नहीं रहना चाहिए । यही इसका मुख्य उद्देश्य है।
इस लेख के द्वारा हमारे महान ऋषि मुनियों ने श्राद्ध रूपी अनमोल संस्कृति जो प्रदान की है उस परंपरा को चालू रखने की सद्बुद्धि हो, सभी को उसका लाभ हो, उसी प्रकार श्राद्ध विधि श्रद्धा के साथ कर पाएं, अपने पूर्वजों की और स्वयं की उन्नति हो यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना है । संदर्भ : सनातन संस्था का ग्रंथ ‘ श्राद्व और श्राद्ध के कृति के पीछे का शास्त्र ‘
DISCLAIMER: The author is solely responsible for the views expressed in this article. The author carries the responsibility for citing and/or licensing of images utilized within the text.
